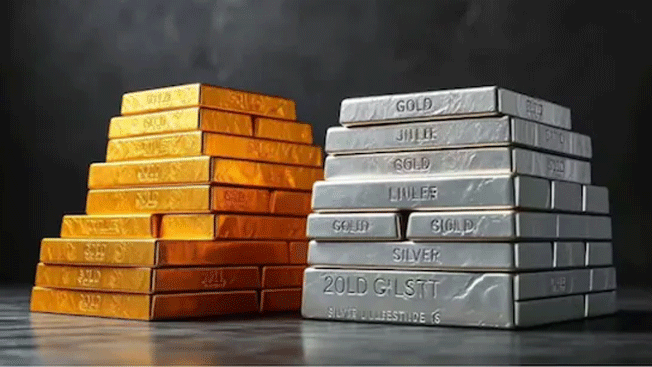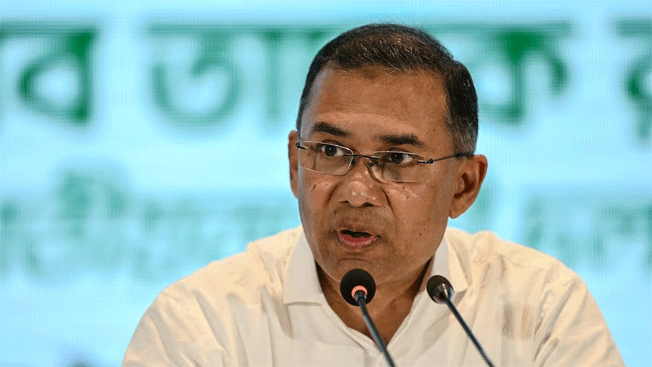भारत की बहु आयामी तपस्विता को एक ब्रह्म करता कुम्भपर्व
भारतीय संस्कृति की सुरभि से विश्व पटल को सुवासित करता महाकुम्भ सनातन पर्व भारतीय तपस्विता के दैहिक दैविक भौतिक सामाजिक व आध्यात्मिक आयाम को संसार के सम्मुख प्रकट कर रहा है । विस्मय से विश्व की आँखे विस्फारित हो चली हैं। विपरीत परिस्थितियों में देह को तपाना दैहिक तपश्चर्या है वह लोक जीवन और सन्यस्थ जीवन दोनो में द्विआयामी दिखाई दे रही है। समस्त भौतिक वैभव को तजती मानवता जिस संपूर्ण सत्य की खोज में यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी वह अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ एक स्थल पर कल्पवास को आतुर है। चिंतन मंथन जिज्ञासा विवेचना का निर्मल आनंद चरम पर है। अस्ति अर्थात जिसका अस्तित्व है उससे अधिक नास्ति जो दिखाई नहीं दे रहा उसका सौंदर्य बहुगुणित होता जा रहा है।अमृत के घट से छलकी वह बूँद जैसे दिव्यता के सागर की होड़ कर रही है जन समूह का समुद्र उस दिव्यता के सागर में समाने को आतुर है । देह घट में उपस्थित जीव घट इस महाकुंभ घट में जो घट रहा है उस घटना पर दार्शनिक दृष्टि का निर्मल आलेपन अनुभव कर रहा है।
दूरदर्शी होने के लिए दृष्टि उदार होना आवश्यक है दिव्य दर्शी होने के लिए उपकार बुद्धि अर्थात कृतज्ञता आवश्यक है इसी उदाहरण का प्रस्तुत प्रसंग है कुम्भ पर्व। ।
भारत में मनाया जा रहा महाकुंभ पर्व द्वादश आवर्तन पूर्ण करते हुए 144 वर्ष के महा योग को साथ ले कर आया है। प्रतिभासित युग में समस्त विश्व प्रयागराज तीर्थ में प्रतिभासित स्नान कर रहा है और गूगल प्रतिभासित पुष्पवर्षा भी कर रहा है । प्रयाग राज में डुबकी लगाकर इस क्षण को साकार जीने वालों की संख्या भी करोड़ों में कही जा रही है । भारत की धरती विश्व के सम्यक समागम का केन्द्र बनी हुई है । न कोई जात पूछ रहा है न ज्ञान । न सेवा भावना में कमी है न आस्था में ।
विश्व की सर्वथा प्राचीन सभ्यता अपनी परंपरा के महा उत्सव में सहगामी होने को आकुल त्रिवेणी के संगम की ओर बढ़ती चली आ रही है। समय के ताल पर अपनी गागर में सागर भर लेने को आतुर आस्था का महानृत्य है यह उत्सव ।
कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः
मूले तत्र स्थितौ ब्रहमा मध्ये मातृगणा स्मृता
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः
अंगेश्च संहिता सर्वे कलशम् तु समाश्रितः
जिस अमृत कलश का उल्लेख किया गया है यह उसकी दिव्यता का वर्णन ही है कि ब्रह्मा विष्णु शिव एवं शक्ति समेत सप्त द्वीप सप्त समुद्र चतुर्वेद संहिताएँ अपने अंगों अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छन्द निरुक्त समेत इस कुम्भ में विद्यमान हैं।
यह कुम्भ पूजन श्लोक भारतीय सांस्कृतिक मंगल बोध का परिचायक है। एक ओर प्रत्येक मांगलिक कार्य में कुम्भ की प्रतिष्ठापना सर्वप्रथम की जाती है। सप्तधान्य के ऊपर सप्त तीर्थों औषधियों से संपन्न जल अथवा अक्षत से पूरकर सप्तपर्ण के साथ मानव मस्तिष्क का प्रतीक नारियल उसके मस्तक पर रख कर , पूर्णत्व की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में उसका मंगलदायी स्थापन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर क्षीर सागर के मन्थन से निकला कुम्भ अमृत से लबालब भरा होने पर जरा सा छलक जाता है तो उसकी अमृत बूंदें मानवता के मोक्ष लक्ष्य की दायिनी बन कर पुण्य दायी पर्व का स्थापन करती हैं।
भारतीय दर्शन में मानव के सर्वोच्च जीवन लक्ष्यों का जब भी उल्लेख होता है घट को साक्ष्य एवं बिम्ब बना कर दर्शन के गूढ प्रश्न स्वं अवधारणाएँ सरलता से समझा दी गई हैं।
‘या घट भीतर पारस मोती याही में परखनहारा’ कह कर संपूर्ण कबीरी निर्लिप्तता में मानव देह के कुंभ को ईश्वर का मंदिर बता दिया गया है।
यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे कह कर संसार को भी घट बता दिया गया। भारतीय आर्ष मनीषी ने कुम्भ के विराट बिम्ब को रचते हुए उपनिषद के शांति पाठ में ऊं पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्प पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्पते के द्वारा ईश्वर की भव्य अवधारणा कितनी सरलता से हमारे सम्मुख रख दी है कि यह घट पूर्ण है वह घट भी पूर्ण है । पूर्ण से ही पूर्ण की रचना होती है। तथा उस परम संपूर्ण में से पूर्ण के रच दिए जाने पर जो शेष बचता है वह भी पूर्ण ही है। . . .
अमृत कलश की छलकती बूंदों से पवित्र हुई चार पुरियों में शाश्वत काल से मनता चला आ रहा कुंभ उत्सव भारतीय प्राचीन सभ्यता की जीवन्त उत्सवधर्मिता का प्रतीक है। देवों और दानवों के द्वारा मंथन किए जाने पर निकले अमृत घट के पूर्व निकले हालाहल विष का पान करने वाले शिव का लोक कल्याण कारी स्वरूप यह संदेश देता है कि अमृतत्त्व तो विषपायी के लोक कल्याण भाव में है । परहित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीड़ा सम नहिं अधमाई
कुंभ का उत्सव अमृत के तत्व को आत्मसात करने का पर्व है। भारत की आध्यात्मिक मेधा अपनी तपस्विता के एकाकी क्रियान्वयन को त्याग कर 45 दिनों के लिए शास्त्रार्थ , चिंतन , मंथन की कामना से आध्यात्मिक संसद में एकत्र होती है। कदाचित पूज्यपाद आदिशंकराचार्य जी भी इसी कामना को आधार रख कर मानवता को सामूहिक मानस मंथन कर आध्यात्म का नवनीत निकालने की प्रेरणा दे गए हैं। भारतीय प्रज्ञा अमृत के महत्व को समझती है वह जन्म से ही मोक्ष की कामना को समझते हुए परिपक्व होती है क्योंकि उसे शैशव काल में वैदिक वाङ्गमय स्वरूप बीज ग्रंथ मिले हैं और बाल्य काल में रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य मिले हैं । विश्व गुरु कहलाने वाली यह सभ्यता सनातन काल से धर्म द्वारा अनुशासित है।
भारतीय दर्शन में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता एवं ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार आदिशंकराचार्य ने इसे वेद व्रती संस्कृति को पुनः पुनः मानस मंथन कर अमृत रूपी दिव्य सत्व की बूंद आत्मसात करने का सुंदर प्रयोजन स्थल कहा है। सत्य है कि प्रथम जिज्ञासा, पश्चात परिवर्तन फिर नवाचार की प्रक्रिया हर युग को नव निर्मिति का संदेश देती चलती है कि अतीत के सत्य को अपना लो फिर इसे शिव अर्थात कल्याणकारी वर्तमान में बदलो जिससे भविष्य स्वतः सुन्दर हो जाए ।
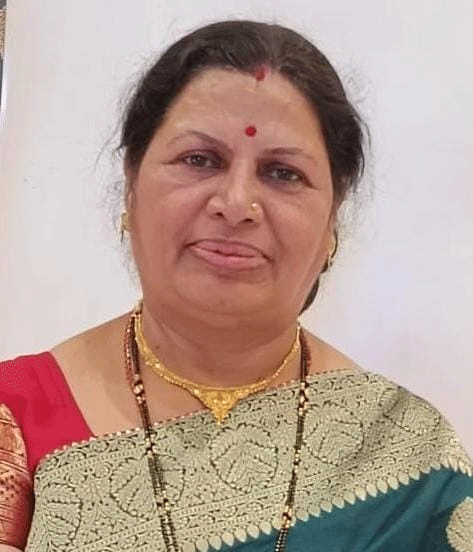
डॉ आरती दुबे
साहित्यकार एवं शिक्षाविद्
drarteedubey@gmail.com